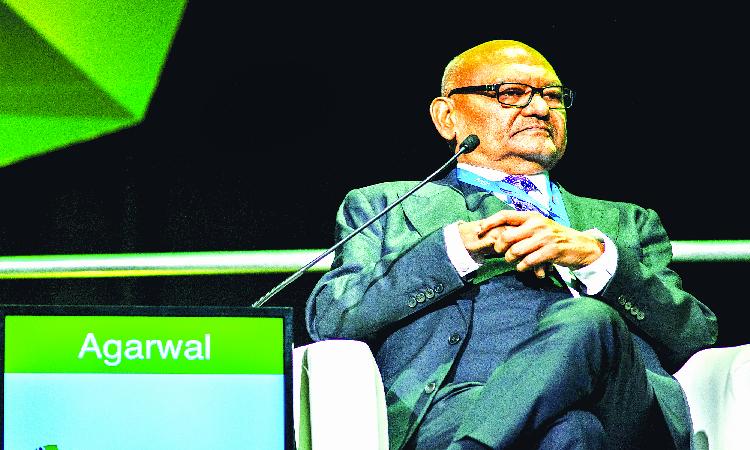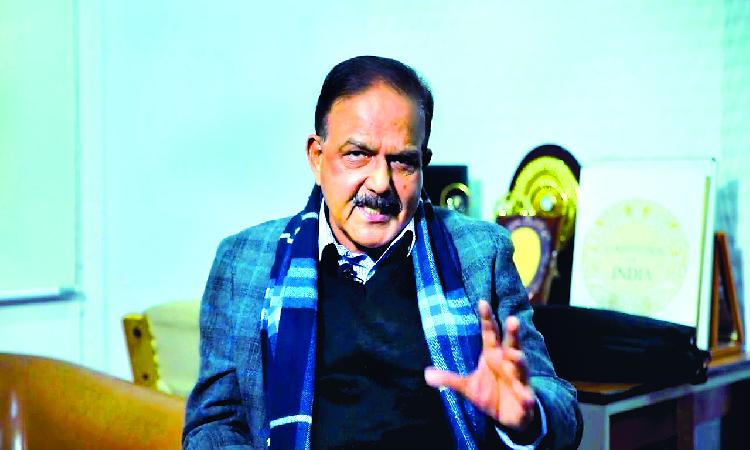जल तनाव के जाल में है पूरा देश

अनिता वेदांडे की रिपोर्ट
पानी को तरस रहे हैं लोग. देश में पानी न सिर्फ एक बुनियादी सवाल है बल्कि पानी का बाजार हर आम और खास को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया है. धरती के नीचे का जलस्तर लगभग हर राज्यों में तेजी से गिर रहा है. नदी, झील, झरना सब सूख रहे हैं। पानी पर बातें तो होती हैं लेकिन इस समस्या को लेकर ठोस कुछ नहीं हो रहा है.
जल तनाव व जल जोखिम
जल तनाव या ‘वाटर स्ट्रेस’ की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी अवधि में जल की मांग उपलब्ध जल की मात्रा से अधिक हो जाती है या जब जल की खराब गुणवत्ता इसके उपयोग को प्रतिबंधित कर देती है.
जल तनाव के घटक
जल जोखिम बिगड़ते जल स्वास्थ्य और अक्षम जल शासन के कारण किसी जल निकाय के समक्ष उत्पन्न जल-संबंधी चुनौती (जैसे जल की कमी, जल तनाव, बाढ़, अवसंरचना का क्षय, सूखा आदि) की संभावना को संदर्भित करता है.
फाल्केनमार्क इंडिकेटर या वाटर स्ट्रेस इंडेक्स : यह किसी देश में ताजे जल की कुल मात्रा को उसकी कुल आबादी से सह संबद्ध करता है और उस दबाव को इंगित करता है जो आबादी द्वारा (पारिस्थितिक तंत्र की आवश्यकताओं सहित) जल संसाधनों पर डाला जाता है.
किसी देश में यदि प्रति व्यक्ति नवीकरणीय जल की मात्रा
- 1,700 घन मीटर से कम हो तो माना जाता है कि वह देश जल तनाव का सामना कर रहा है.
- 1,000 घन मीटर से कम हो तो माना जाता है कि वह देश जल की कमी का सामना कर रहा है.
- 500 घन मीटर से कम हो तो माना जाता है कि वह देश जल की पूर्ण कमी का सामना कर रहा है.
- भारत में जल प्रबंधन की स्थिति
- वर्तमान स्थिति: भारत विश्व में भूजल का सबसे अधिक निष्कर्षण करता है. यह मात्रा विश्व के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े भूजल निष्कर्षण-कर्ता (चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका) के संयुक्त निष्कर्षण से भी अधिक है.
- हालांकि भारत में निष्कर्षित भूजल का केवल 8% ही पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है.
- इसका 80% भाग सिंचाई में उपयोग किया जाता है.
- नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक ने भारत में उभरते जल संकट के बारे में आगाह किया है जहाँ देश के 600 मिलियन से अधिक लोग जल की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं.
- यह आकलन भी किया गया है कि वर्ष 2030 तक देश की जल मांग उपलब्ध आपूर्ति की तुलना में दोगुनी हो जाएगी।
गर्मी आई, पानी की आफत लाई
युक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट, 2022 के अनुसार जलधाराओं, झीलों, जलभृतों और मानव-निर्मित जलाशयों से ताजे जल की तेजी से निकासी के साथ-साथ विश्व भर में आसन्न जल तनाव और जल की कमी के संबंध में वैश्विक चिंता बढ़ती जा रही है. बदलती जलवायु प्रवृत्तियों, बार-बार उभर रही प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों की अचानक तेज वृद्धि से यह स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है. 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर भारत के संक्रमण में सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना सर्वोपरि है. इस प्रयास में जल एक महत्त्वपूर्ण संसाधन होने की भूमिका रखता है. विश्व की लगभग 17% आबादी का वहन करने वाला भारत विश्व के ताजे जल संसाधनों का मात्र 4% ही रखता है, जो स्पष्ट रूप से इसके विवेकपूर्ण उपयोग और कुशल जल जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर करता है.
कुछ प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद हैं
- कृष्णा नदी : महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना
- कावेरी नदी : केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी
- पेरियार नदी : तमिलनाडु, केरल
- नर्मदा नदी : मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान
अप्रभावी अपशिष्ट जल प्रबंधन
अत्यधिक जल-तनाव के परिदृश्य में अपशिष्ट जल का अप्रभावी उपयोग भारत को अपने जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग कर सकने में असमर्थ बना रहा है. शहरों में यह जल मुख्यत: ‘ग्रेवाटर’ के रूप में पाया जाता है.
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हाल में प्रकाशित एक रिपोर्ट (मार्च 2021) के अनुसार, भारत की वर्तमान जल उपचार क्षमता 27.3% और सीवेज उपचार क्षमता 18.6% है (जहाँ अतिरिक्त 5.2% क्षमता जोड़ी जा रही है). लेकिन फिर भी अधिकांश सीवेज उपचार संयंत्र अधिकतम क्षमता पर कार्य नहीं कर रहे हैं और निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं.
- खाद्य सुरक्षा जोखिम: फसल और पशुधन उत्पादन के लिये जल आवश्यक है. कृषि में सिंचाई के लिये जल का वृहत उपयोग किया जाता है और जल घरेलू उपभोग का भी एक प्रमुख स्रोत है. तेजी से गिरते भूजल स्तर और अक्षम नदी जल प्रबंधन के संयोजन से खाद्य असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.
- जल एवं खाद्य की कमी के उत्पन्न प्रभाव आधारभूत आजीविका को जटिल कर सकते हैं और सामाजिक तनाव को बढ़ा सकते हैं.
- बढ़ता जल प्रदूषण: घरेलू, औद्योगिक और खनन अपशिष्टों की एक बड़ी मात्रा जल निकायों में बहाई जाती है, जिससे जलजनित रोग उत्पन्न हो सकते हैं. इसके अलावा, जल प्रदूषण से सुपोषण या यूट्रोफिकेशन की स्थिति बन सकती है जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है।
- भूजल का अत्यधिक दोहन: केंद्रीय भूजल बोर्ड के नवीनतम अध्ययन के अनुसार भारत के 700 जिलों में से 256 जिलों ने गंभीर या अत्यधिक दोहित भूजल स्तर की सूचना दी है।
- अति-निर्भरता और निरंतर खपत के कारण भूजल संसाधनों पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप कुएँ, पोखर, तालाब आदि सूख रहे हैं। इससे जल संकट गहरा होता जा रहा है
Recent Posts
समाज के नायक
Latest breaking news and special reports